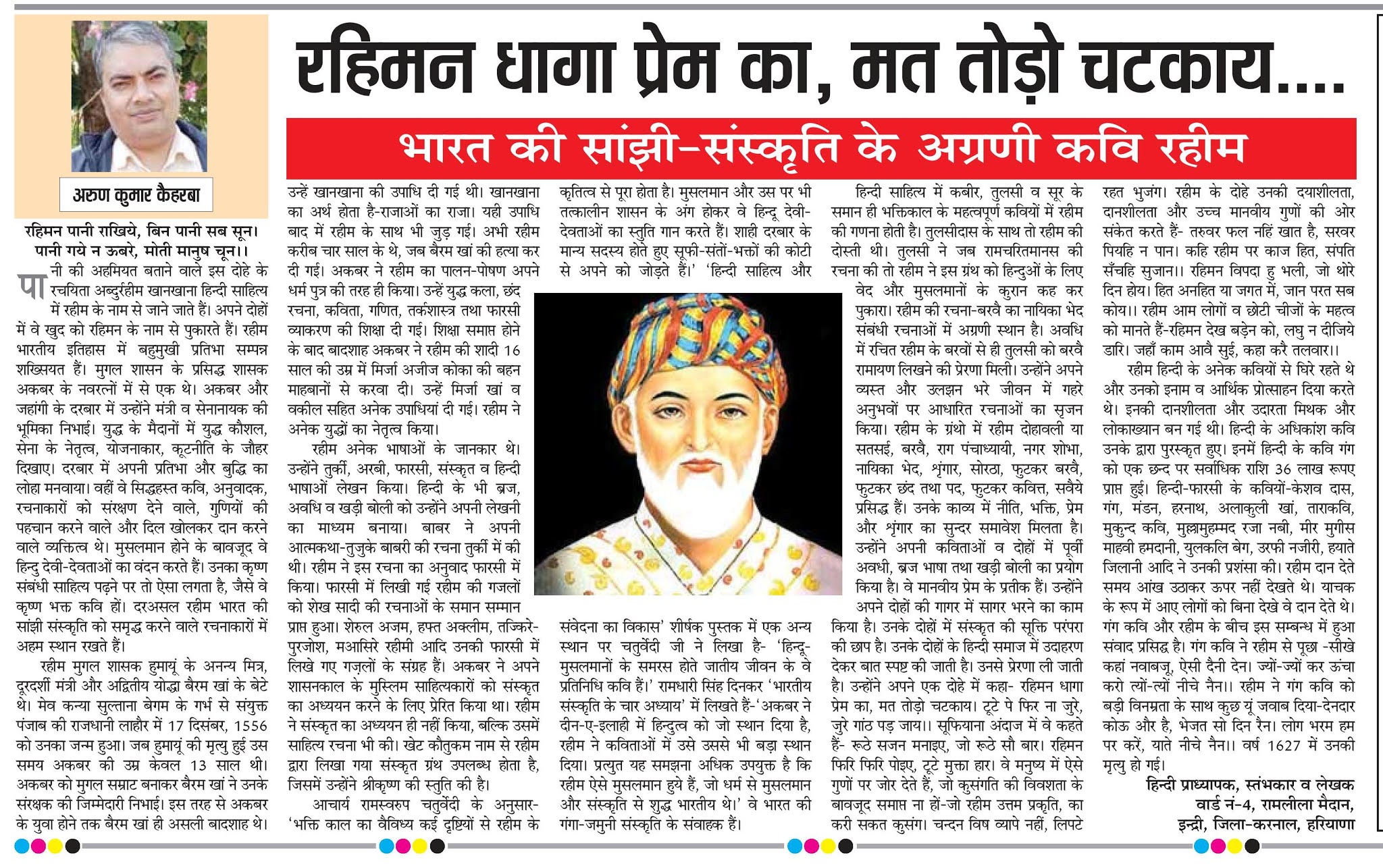जयंती विशेष
तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे.. ..
शहंशाहे तरन्नुम मोहम्मद रफी ने पाश्र्व गायन को दिए नए आयाम
अरुण कुमार कैहरबा
 |
| dainik purvodya 24-12-2020 |
‘तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग-संग तुम भी गुनगुनाओगे।’
मोहम्मद रफी द्वारा गाया गया यह गीत सदा सच रहेगा। संगीत की दुनिया में उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी आवाज़ का जादू संगीत प्रेमियों के अहसास में रचा-बसा है। मोहम्मद रफी द्वारा गाए गए हज़ारों गाने आज भी उसी शिद्दत से बजाए और गाए जाते हैं, जैसे वर्षों पहले गाए-बजाए जाते थे और आने वाले वर्षों में भी उन्हें इसी तरह पसंद किया जाता रहेगा। र$फी ने हिन्दी फिल्मों में रोमांटिक गीतों के अलावा ग़ज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली सहित अनेक विधाओं में गीत गाए हैं। इन गीतों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विभिन्न अभिनेताओं पर फिल्माए गए गीतों के मिजाज़ और आवाज़ में भी अभिनेताओं के स्वभाव व अभिनय की खूबियों के अनुसार ही अंतर पैदा किया गया है। हिन्दी सिनेमा के श्रेष्ठतम पाश्र्व गायक को संगीत प्रेमियों ने शहंशाह-ए-तरन्नुम के सम्मान से नवाजा है।
अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसम्बर, 1924 को हुआ। इनके परिवार का संगीत से कोई विशेष जुड़ाव नहीं था। उनके वालिद हाजी अली मोहम्मद साहब दीनी-इन्सान थे। वे गाने-बजाने को अच्छा नहीं मानते थे। रफी ने कम उम्र में ही गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था। रफी के बड़े भाई मोहम्मद दीन की नाई की दुकान थी। दुकान के पास से ही गाता हुआ एक फकीर गुजरता था। र$फी को फकीर की आवाज पसंद आई और वह फकीर की आवाज सुनने के लिए उनका पीछा करने लगे। उसी फकीर की नकल करते हुए र$फी ने गाना शुरू किया। र$फी गाते तो दुकान पर आए लोग उनकी तारीफ करते। लेकिन यह सब वे अपने अब्बू जी से छिप-छिप कर ही करते थे।
11 साल की उम्र में रफी का परिवार लाहौर चला गया। वहां पर बड़े भाई मोहम्मद दीन के दोस्त हमीद ने र$फी की प्रतिभा की पहचान की और उसे प्रोत्साहन दिया। वे रफी को अपने समय के कुछ उस्तादों के पास ले गए। र$फी को 13साल की उम्र में उस वक्त सार्वजनिक मंच पर गाने का अवसर मिला, जब ऑल इंडिया रेडियो लाहौर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक-अभिनेता कुंदन लाल सहगल गाने के लिए आए थे। मोहम्मद र$फी वहीद के साथ उन्हें सुनने के लिए गए थे। ऐन मौके पर बिलजी गुल हो गई। बिजली नहीं होने के कारण बिना माइक के सहगल साहब का गाना संभव नहीं था। ऐसे में हमीद ने आयोजकों से र$फी को गाने का मौका देने का अनुरोध किया, जिसे मान लिया गया। वहीं पर मौजूद प्रसिद्ध संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें गाने का न्यौता दिया। इस प्रकार 1941 में उन्हीं के निर्देशन में बन रही पंजाबी फिल्म ‘गुल बलोच’ में र$फी को अपना पहला गीत गाने का मौका मिला। फिल्म में जीनत बेगम के साथ गाया गया युगल गीत- सोनिए हीरीए उनका पहला गीत था।
र$फी 1944 में अपने सरपरस्त हमीद साहब के साथ बम्बई में आ गए। बंबई के भिंडी बाजार में छोटे से कमरे में उभरते हुए गायक रफी रहे। श्याम सुंदर भी बंबई में आ गए थे। पुराने परिचय के कारण वे ही पहली बार उनके काम आए। उन्होंने फिल्म गांव की गोरी में रफी साहब से बंबई का पहला गाना गवाया। हालांकि इसी साल संगीतकार नौशाद ने भी उन्हें गाने का मौका दिया। 1947 में दिलीप कुमार व नूरजहाँ अभिनीत फिल्म जुगनू में गीत-यहां बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है ने रफी साहब को स्टार सिंगर बना दिया। फिल्म बैजू बावरा के गीतों से भी र$फी को ख्याति मिली। 1947 में देश के बंटवारे के दौरान रफी साहब ने बंबई में ही रहने का फैसला किया और लाहौर में रह रहे अपने परिवार को भी यहीं बुला लिया। 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद राजेन्द्र कृष्ण द्वारा लिखे गए गीत- ‘सुनो-सुनो ऐ दुनिया वालो बापू की ये अमर कहानी’ रफी साहब ने समारोह में गाया। प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने गीत सुना तो उन्होंने रफी को अपने घर होने वाली श्रद्धांजलि सभा में गीत गाने के अनुरोध के साथ बुलाया। आजादी का एक साल पूरा होने पर समारोह में नेहरू ने रफी को मेडल से सम्मानित किया।
राज कपूर के पसंदीदा संगीतकार शंकर-जयकिशन की जोड़ी मुकेश की आवाज पर भरोसा करती थी। बाद में उन्हें भी र$फी की आवाज पसंद आई। इसके बाद सचिन देव बर्मन, ओ.पी. नैय्यर, रवि, मदन मोहन, गुलाम हैदर, जयदेव व सलिल चौधरी सहित अनेक संगीतकारों के साथ र$फी ने काम किया। हजारों गीत गाएं। रफी की गायिकी की जितनी तारीफ की जाए कम है। वे भजन, $गज़ल, कव्वाली, देश भक्ति गीत, रोमांटिक गीत, मनचला गीत, क्लब का गीत, उदास गीत जो भी गाएं, वहीं आवाज का जादू बिखेर देते हैं। वे फिल्म निर्देशक, संगीतकार, अभिनेता सभी के रंगों में रंग जाते हैं। इससे पहले फिल्म में गायकों को ही अभिनेता के रूप में लिया जाता था। सहगल, सुरैया, नूरजहाँ आदि ने गायक और अभिनेता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। मोहम्मद रफी ने पाश्र्व गायन को नया रंग और नए आयाम दिए।
हर अभिनेता के व्यक्तित्व व स्वभाव के हिसाब से मोहम्मद रफी ने गायिकी को अलग अंदाज दिया। नैन लड़ जहिएं तो मनवा मा खटक होईबे करी, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, ये चांद सा रोशन चेहरा, दीवाना हुआ बादल, परदेसियों से ना अखियां मिलाना.., सुख के सब साथी..., जो वादा किया वो..., दिन ढ़ल जाए हाए.., इस रंग बदलती दुनिया में, तेरी प्यारी-प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, याद ना जाए बीते दिनों की, सुहानी रात ढ़ल चुकी, तेरे-मेरे सपने.., हर फिक्र को धुएं मेंं उड़ता चला गया और लिखे जो ख़त तुझे...सहित कितने ही गीत र$फी की मखमली आवाज के साथ आज भी लोगों की जुबान पर हैं। मन तड़पत हरी दर्शन को आज, मधुबन में राधिका नाचे रे, ओ दुनिया के रखवाले सहित कितने ही गाने उनके उत्कृष्ट गायन के उदाहरण हैं। गंभीर, रोमानी, देशभक्ति और भक्ति के गीतों के साथ ही बहुत से गीतों में उनकी बच्चों सी चंचलता व नटखटपन भी मुखर हो जाती है। इनमें ‘रे माम्मा रे माम्मा रे, रे माम्मा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुडिय़ों की रानी’ एक मिसाल है। रफी साहब को छह बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला। 1960 में फि़ल्म ‘चौदहवीं का चांद’ के शीर्षक गीत के लिए रफ़ी को अपना पहला फि़ल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फि़ल्मफेयर आवार्ड फि़ल्म ‘ससुराल’ के गीत ‘तेरी प्यारी प्यारी सूरत को’ के लिए मिला। 1965 में ही लक्ष्मी-प्यारे के संगीत निर्देशन में फि़ल्म ‘दोस्ती’ के लिए गाए गीत- ‘चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे’ के लिए रफ़ी को तीसरा फि़ल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1966 में फि़ल्म ‘सूरज’ के गीत बहारों फूल बरसाओ बहुत प्रसिद्ध हुआ और इसके लिए उन्हें चौथा फि़ल्मफेयर अवार्ड मिला। इसका संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। 1968 में शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में फि़ल्म ‘ब्रह्मचारी’ के गीत दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर के लिए उन्हें पाचवां फि़ल्मफेयर अवार्ड मिला। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। आवाज के साथ दुनिया को सुंदर गानों की सौगात देने वाले र$फी साहब 31जुलाई, 1980 को दुनिया से तो चल बसे। लेकिन उनकी आवाज का जादू ना कभी कम हुआ और ना होगा। दिल का सूना साज़ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज़ निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा।
अरुण कुमार कैहरबा,
हिन्दी प्राध्यापक, संस्कृतिकर्मी, स्तंभकार, लेखक
वार्ड नं.-4, रामलीला मैदान, इन्द्री
जिला-करनाल, हरियाणा
मो.नं.-94662-20145
navsatta 
vir arjun 
tarun mitr
 |
| jammu parivartan |
 |
| prakhar vikas |