भारत की सांझी-संस्कृति के अग्रणी कवि रहीम
अरुण कुमार कैहरबा
रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती मानुष चून।। पानी की अहमियत बताने वाले इस दोहे के रचयिता अब्दुर्रहीम खानखाना हिन्दी साहित्य में रहीम के नाम से जाने जाते हैं। अपने दोहों में वे खुद को रहिमन के नाम से पुकारते हैं। रहीम भारतीय इतिहास में बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न शख्सियत हैं। मुगल शासन के प्रसिद्ध शासक अकबर के नवरत्मों में से एक थे। अकबर और जहांगी के दरबार में उन्होंने मंत्री व सेनानायक की भूमिका निभाई। युद्ध के मैदानों में युद्ध कौशल, सेना के नेतृत्व, योजनाकार, कूटनीति के जौहर दिखाए। दरबार में अपनी प्रतिभा और बुद्धि का लोहा मनवाया। वहीं वे सिद्धहस्त कवि, अनुवादक, रचनाकारों को संरक्षण देने वाले, गुणियों की पहचान करने वाले और दिल खोलकर दान करने वाले व्यक्तित्व थे। मुसलमान होने के बावजूद वे हिन्दु देवी-देवताओं का वंदन करते हैं। उनका कृष्ण संबंधी साहित्य पढऩे पर तो ऐसा लगता है, जैसे वे कृष्ण भक्त कवि हों। दरअसल रहीम भारत की सांझी संस्कृति को समृद्ध करने वाले रचनाकारों में अहम स्थान रखते हैं।रहीम मुगल शासक हुमायूं के अनन्य मित्र, दूरदर्शी मंत्री और अद्वितीय योद्धा बैरम खां के बेटे थे। मेव कन्या सुल्ताना बेगम के गर्भ से संयुक्त पंजाब की राजधानी लाहौर में 17 दिसंबर, 1556 को उनका जन्म हुआ। जब हुमायूं की मृत्यू हुई उस समय अकबर की उम्र केवल 13 साल थी। अकबर को मुगल सम्राट बनाकर बैरम खां ने उनके संरक्षक की जिम्मेदारी निभाई। इस तरह से अकबर के युवा होने तक बैरम खां ही असली बादशाह थे। उन्हें खानखाना की उपाधि दी गई थी। खानखाना का अर्थ होता है-राजाओं का राजा। यही उपाधि बाद में रहीम के साथ भी जुड़ गई। अभी रहीम करीब चार साल के थे, जब बैरम खां की हत्या कर दी गई। अकबर ने रहीम का पालन-पोषण अपने धर्म पुत्र की तरह ही किया। उन्हें युद्ध कला, छंद रचना, कविता, गणित, तर्कशास्त्र तथा फारसी व्याकरण की शिक्षा दी गई। शिक्षा समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर ने रहीम की शादी 16 साल की उम्र में मिर्जा अजीज कोका की बहन माहबानों से करवा दी। उन्हें मिर्जा खां व वकील सहित अनेक उपाधियां दी गई। रहीम ने अनेक युद्धों का नेतृत्व किया।
रहीम अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने तुर्की, अरबी, फारसी, संस्कृत व हिन्दी भाषाओं लेखन किया। हिन्दी के भी ब्रज, अवधि व खड़ी बोली को उन्होंने अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। बाबर ने अपनी आत्मकथा-तुजुके बाबरी की रचना तुर्की में की थी। रहीम ने इस रचना का अनुवाद फारसी में किया। फारसी में लिखी गई रहीम की गजलों को शेख सादी की रचनाओं के समान सम्मान प्राप्त हुआ। शेरुल अजम, हफ्त अक्लीम, तज्किरे-पुरजोश, मआसिरे रहीमी आदि उनकी फारसी में लिखे गए गज़लों के संग्रह हैं। अकबर ने अपने शासनकाल के मुस्लिम साहित्यकारों को संस्कृत का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। रहीम ने संस्कृत का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसमें साहित्य रचना भी की। खेट कौतुकम नाम से रहीम द्वारा लिखा गया संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध होता है, जिसमें उन्होंने श्रीकृष्ण की स्तुति की है।
आचार्य रामस्वरुप चतुर्वेदी के अनुसार- ‘भक्ति काल का वैविध्य कई दृष्टियों से रहीम के कृतित्व से पूरा होता है। मुसलमान और उस पर भी तत्कालीन शासन के अंग होकर वे हिन्दू देवी-देवताओं का स्तुति गान करते हैं। शाही दरबार के मान्य सदस्य होते हुए सूफी-संतों-भक्तों की कोटी से अपने को जोड़ते हैं।’ ‘हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास’ शीर्षक पुस्तक में एक अन्य स्थान पर चतुर्वेदी जी ने लिखा है- ‘हिन्दू-मुसलमानों के समरस होते जातीय जीवन के वे प्रतिनिधि कवि हैं।’ रामधारी सिंह दिनकर ‘भारतीय संस्कृति के चार अध्याय’ में लिखते हैं-‘अकबर ने दीन-ए-इलाही में हिन्दुत्व को जो स्थान दिया है, रहीम ने कविताओं में उसे उससे भी बड़ा स्थान दिया। प्रत्युत यह समझना अधिक उपयुक्त है कि रहीम ऐसे मुसलमान हुये हैं, जो धर्म से मुसलमान और संस्कृति से शुद्ध भारतीय थे।’ वे भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति के संवाहक हैं।
हिन्दी साहित्य में कबीर, तुलसी व सूर के समान ही भक्तिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में रहीम की गणना होती है। तुलसीदास के साथ तो रहीम की दोस्ती थी। तुलसी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो रहीम ने इस ग्रंथ को हिन्दुओं के लिए वेद और मुसलमानों के कुरान कह कर पुकारा। रहीम की रचना-बरवै का नायिका भेद संबंधी रचनाओं में अग्रणी स्थान है। अवधि में रचित रहीम के बरवों से ही तुलसी को बरवै रामायण लिखने की प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने व्यस्त और उलझन भरे जीवन में गहरे अनुभवों पर आधारित रचनाओं का सृजन किया। रहीम के ग्रंथो में रहीम दोहावली या सतसई, बरवै, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, शृंगार, सोरठा, फुटकर बरवै, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्त, सवैये प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और शृंगार का सुन्दर समावेश मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं व दोहों में पूर्वी अवधी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया है। वे मानवीय प्रेम के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने दोहों की गागर में सागर भरने का काम किया है। उनके दोहों में संस्कृत की सूक्ति परंपरा की छाप है। उनके दोहों के हिन्दी समाज में उदाहरण देकर बात स्पष्ट की जाती है। उनसे प्रेरणा ली जाती है। उन्होंने अपने एक दोहे में कहा- रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाय।। सूफियाना अंदाज में वे कहते हैं- रूठे सजन मनाइए, जो रूठे सौ बार। रहिमन फिरि फिरि पोइए, टूटे मुक्ता हार। वे मनुष्य में ऐसे गुणों पर जोर देते हैं, जो कुसंगति की विवशता के बावजूद समाप्त ना हों-जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। चन्दन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीम के दोहे उनकी दयाशीलता, दानशीलता और उच्च मानवीय गुणों की ओर संकेत करते हैं- तरुवर फल नहिं खात है, सरवर पियहि न पान। कहि रहीम पर काज हित, संपति सँचहि सुजान।। रहिमन विपदा हु भली, जो थोरे दिन होय। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय।। रहीम आम लोगों व छोटी चीजों के महत्व को मानते हैं-रहिमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिये डारि। जहाँ काम आवै सुई, कहा करै तलवार।।
 |
| दैनिक प्रखर विकास |
रहीम हिन्दी के अनेक कवियों से घिरे रहते थे और उनको इनाम व आर्थिक प्रोत्साहन दिया करते थे। इनकी दानशीलता और उदारता मिथक और लोकाख्यान बन गई थी। हिन्दी के अधिकांश कवि उनके द्वारा पुरस्कृत हुए। इनमें हिन्दी के कवि गंग को एक छन्द पर सर्वाधिक राशि 36 लाख रूपए प्राप्त हुई। हिन्दी-फारसी के कवियों-केशव दास, गंग, मंडन, हरनाथ, अलाकुली खां, ताराकवि, मुकुन्द कवि, मुल्लामुहम्मद रजा नबी, मीर मुगीस माहवी हमदानी, युलकलि बेग, उरफी नजीरी, हयाते जिलानी आदि ने उनकी प्रशंसा की। रहीम दान देते समय आंख उठाकर ऊपर नहीं देखते थे। याचक के रूप में आए लोगों को बिना देखे वे दान देते थे। गंग कवि और रहीम के बीच इस सम्बन्ध में हुआ संवाद प्रसिद्घ है। गंग कवि ने रहीम से पूछा -सीखे कहां नवाबजू, ऐसी दैनी देन। ज्यों-ज्यों कर ऊंचा करो त्यों-त्यों नीचे नैन।। रहीम ने गंग कवि को बड़ी विनम्रता के साथ कुछ यूं जवाब दिया-देनदार कोऊ और है, भेजत सो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन।। वर्ष 1627 में उनकी मृत्यु हो गई।
अरुण कुमार कैहरबा,
हिन्दी प्राध्यापक, स्तंभकार व लेखक
वार्ड नं-4, रामलीला मैदान,
इन्द्री, जिला-करनाल, हरियाणा
मो.नं.-09466220145
 |
| दैनिक नवसत्ता |
 |
| दैनिक पूर्वोदय |




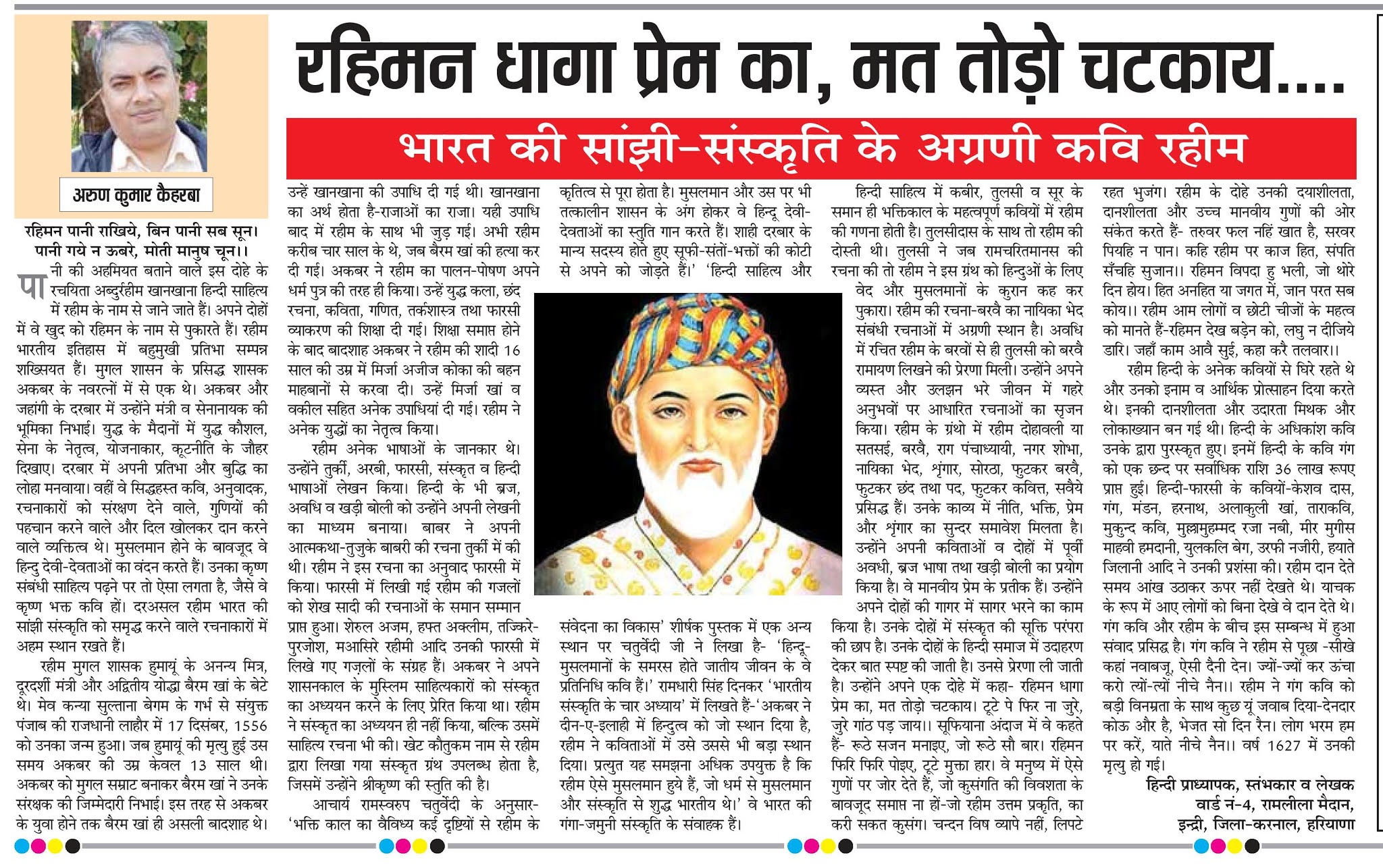

No comments:
Post a Comment